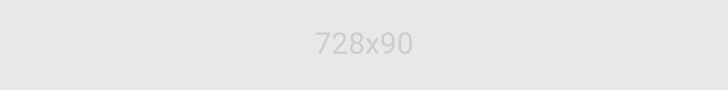पृथ्वी दिवस: असंतुलित विकास और पर्यावरण
पर्यावरण संकट भौगोलिक सीमाओं को चीर कर जीवन को चुनौती दे रहा है। ग्लोबल वार्मिग, ओजोन परत के संरक्षण, मौसमी बदलाव, जलवायु परिवर्तन, भूक्षरण, मिट्टी की नमी, सतहीजल, सतह के नीचे का जल, नमी संरक्षण की समस्यायें मुॅह बाये खड़ी हैं। वायु, जल, पृथ्वी प्रदूषण से ग्रसित होते जा रहे हैं। वनस्पतियॉ व पक्षियों की प्रजातियॉ लुप्त और कम हो रही हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में कामयाबी नहीं मिल रही है। कार्बन डाई आक्साईड व सल्फर डाई आक्साईड जैसी गैसों का उत्सर्ग बढ़ रहा है।
नदियों, झीलों, वन्य प्राणियों, वनस्पतियों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण के खतरे प्रत्येक प्राणी के सामनें उपस्थित हैं। समुद्री जल स्तर खतरे का संकेत दे रहा है। भू-जल स्तर गिर रहा हैं, बढ़ते प्रदूषण के कारण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा हो रही है। सूखा व बाढ की स्थितियॉ अधिक आने लगी हैं। गर्मी व पानी के प्रदूषण से बीमारियॉ बढ रही हैं। निर्माण, औद्योगिकरण व विकास के नाम पर असंतुलित शहरी-करण व निर्माण बढ़ रहा है। जंगलों का वे हिसाब व ब़े मिसाल कटाव हुआ है। शहरी व ग्रामीण इलाकों के तापमान में काफी अंतर आया है। बेमौसम बरसात व बर्फ बारी भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि प्रदूषण बढ रहा है।
जमीन के वर्तमान वितरण को देखें तो घोर विषमता फैल रही है। शहर की अधिकांष जमीन सम्पन्न वर्ग के कब्जे में आ रही है। अनियत्रित सीमेंट कोन्क्रीट के निमार्णेां से हरियाली समाप्त हो रही है। आबादी का सबसे गरीब 25 प्रतिषत हिस्सा आवासीय भूमि के सिर्फ 5 प्रतिषत हिस्से पर रह रहा है। कच्ची व गन्दी बस्तियॉ बढ़ रही हैं जो जमीन कम आमदनी वाले गरीबों के लिए आरक्षित थी वह अमीरों की हवेलियों में चली गई है। अमीर व गरीब अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। हम भूल रहे हैं गन्दगी व कचरे के ढेर पर्यावरण के लिए सबसे अधिक घातक हैं। सार्वजनिक हित व सार्वजनिक उपयोग को भुलाया जा रहा है। भूमि की गुणवत्ता, उत्पादकता, सत्त विकास की ओर ध्यान नही है।
विकास क्रम में प्राकृतिक वस्तुओं को नष्ट किया जा रहा है। व्यापार व उद्योग आधारित विकास को विकास का एक मात्र ढ़ांचा मान लिया गया है। हम भूलते जा रहे हैं कि पृथ्वी, पानी, हवा, ध्वनि, आकाष तथा वनस्पति पर्यावरण के मूल आधार हैं। प्राकृतिक संतुलन बिगड रहा है। विकास के नाम पर इन तत्वों को नष्ट किया जा रहा है व अनुपात असंतुलित हो रहा है। शहरीकरण के नाम पर, सडक बनाने, उद्योग लगाने, नगर बसाने के नाम पर जंगलों को बे-हताषा काटा जा रहा है। मोटर गाडियों की संख्या बढ़ रही है जिससे वायु व ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। हम भौतिक विकास को एकमात्र विकास मान रहे हैं, महज पर्यावरण सम्मेलन व पर्यावरण दिवसों का आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण के नाम पर संतुष्ट हो रहे हैं। उपभेाक्तावादी संस्कृति फल फूल रही है।
अर्थ व्यवस्था का संकट गम्भीर और गहरा है। भारत के विकास मार्ग में कई गड्ढे व मोड़ हैं जिससे हमारी महत्वाकांक्षी विकास योजनाऐं अपना उद्देष्य प्राप्त करने में पूर्ण सफल नहीं रही। जन संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, कृषि भूमि कम हो गई और प्रदूषण की चुनौती बढ़ती गई। जीवन को बचाने के लिए कई जटिल समस्यायें पैदा हो गई । आज करीब 15 करोड लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। पॉच साल से कम उम्र के आधे बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं व उनका बजन कम है। 35 प्रतिषत से भी अधिक आबादी एक दिन में एक डालर से भी कम उपार्जित कर रही है। अब तक की प्रगति से बहुत थोडे से लोग लाभान्वित हुये हैं। निष्पादन रणनीति के अभाव में संसाधनों की बर्बादी अधिक हो रही है।
पर्यावारण के खतरे हर देष ही नहीं हर व्यक्ति, हर प्राणी के सामने उपस्थित है। हमें ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन को कम करने में कामयाबी नहीं मिली। लुप्त हो रही प्रजातियां और कम हो रही जैव विविधता की हालत स्पष्ट संकेत दे रही है। वैज्ञानिक ओजोन परत के क्षरण से लेकर ग्लेसियरों के पिघलने तक हमें सावधान कर रहे है। पारम्परिक उर्जा स्त्रोतों के उपयोग से नदियांे, झीलों, वन्य प्राणियों, वनस्पतियों और समुच्य तंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। विकसित देष पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग कर रहे है। आर्कटिक महासागर में बर्फ की सिल्लियों की मोटाई कम हो गई। समुद्री जल स्तर खतरे का संदेष दे रहा है। अण्टार्कटिका में पैंग्वनों की संख्या, मोनार्क तितलियां बीमारी की षिकार हो रही है। समुद्रतल से उंचाई पर बसी भूमियों तक मलेरिया और मादा एनाफलिज का कहर पंहुच चुका है। इण्डोनेषिया में प्राकृतिक कारणों से लाखों एकड़ जंगल जल चुके है। जीव जन्तुओं और वनस्पतियांे की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही है। भूजल का स्तर गिर रहा है। तटीय वनों का सफाया हो रहा है। दुष्परिणाम सुनामी के रूप में देखने को मिला है। समुद्र में स्वच्छ जल का स्तर बढ़ता है, इससे वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा की स्थिति, मीठे पानी के स्त्रोत में खारे पानी की मिलावट बढ़ी है। सूखा और बाढ़ की स्थितियां बनी है। तटीय ष्षहरों के डूबने का खतरा बढ़ रहा है।
भारत की लगभग 6000 किमी. लम्बी तटरेखा है। लगभग एक चौथाई जनसंख्या समुद्रीतट से 50 किमी. के दायरे में रहती है। जलवायु के असंतुलन से फसलों पर असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार बिगड़ते पर्यावरण मंे जिन देषों में सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आंषका है, उनमें भारत भी है, और भारत की पहचान उन 27 राष्ट्रों में है, जिन्हें समुद्री जल स्तर के बढ़ने से ज्यादा खतरा है। पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के लिए जैव विविधता वाले भारत के पर्यावरण को हरा भरा व संरक्षित रखने की आवष्यकता है। पर्यावरणीय खतरा समय के साथ बढ़ रहा है।
संसार की एक तिहाई आबादी विभिन्न महाद्वीपों पर समुद्र से सिर्फ 100 किमी. के दायरे में रहती है। द्विपीय देषों और न्यून भूमियों के संकट कम चिन्ताजनक नहीं है। हमारे यहां सकल वन क्षेत्र अपेक्षित स्तर तक नहीं है। हमारे 72 षहर प्रदूषण की चपेट मंे है। इन नगरों में राष्ट्रीय वायु गुणवता मानदण्डों का उल्लघंन हो रहा है। वायु प्रदूषणों के साथ साथ जल प्रदूषण पर भी नियंत्रण आवष्यक है। परंतु प्रदूषकों व रासायनिक अपषिष्टों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव झीलों को भी झेलने पड़ रहे है। ओजोन प्रकोष्ठ ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए कार्य कर रहा है। परंतु विकसित देष रासायनिक प्रदूषण बढ़ाते रहे है। गैसों के उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसके कारण प्रमुख समास्याऐं ओजोन परत में छिद्र, समुद्री स्तर में वृद्धि, भूजल का विषैली होना, धुव्रों की बर्फ का पिघलना, वन क्षेत्रों का सिकुड़ना, लुप्त प्रायः जीव आदि है।
पर्यावरणीय असन्तुलन प्रत्येक देष व व्यक्ति की समस्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरीजीत पसायत ने कहा है कि ‘‘मैं बड़े व्यवसायों से उपर, सरकार को मानता हूं और सरकार से उपर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। लेकिन इन सबसे उपर पर्यावरण है। पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए साझे प्रयासों की आवष्यकता है।’’
देश की विकास दर को बेहतर बनाये रखते हुए पर्यावरणीय हितों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय लिहाज से बड़ी चुनौती है जीवाश्म-ईंधन आधारित अर्थ व्यवस्था के विकल्प की आवश्यकता है। विकास दर और पर्यावरणीय हितों के बीच कैसे संतुलन और तालमेल बनाया जाय इसकी आवश्यकता है। भारत की अर्थ व्यवस्था केतेज रफ्तार के लिए आवश्यक है कि आवश्यकताओं के अनुरूप ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी हो। ऊर्जा उत्पादन वर्तमान मे ंकोयला समेत अन्य जीवाश्म ईंधनों का दौर है। कोयले का भारत में ऊर्जा उत्पादन में लगभग 53 फीसदी हिस्सा है। उच्च दबाब व डीप वाटर क्षेत्र में गैस उत्पादन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा उत्पादन उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है।
यह संभव नहीं हैं कि उपभेाक्तावादी जीवन षैली अपनाते हुये पर्यावरणीय संतुलन बिगाडा जाता रहे जिससे पर्यावरण संतुलन प्रत्येक व्यक्ति की समस्या बनता जाये। व्यवसाय व निर्माण स्वतंत्रता से ऊपर पर्यावरण को मानना होगा। पृथ्वी पर पैदा होने वाली सभी वन सम्पतियॉ हमें पानी उपलब्ध कराती हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। पानी के अपव्यय को रोकने पर ध्यान देना होगा। नदियॉ, झीलें, पानी का बढ़ा स्त्रोत हैं उनमें बढ़ते प्रदूषण को हमें रोकना होगा। समय आ गया है जब हमें वर्षा का पानी अधिक से अधिक संरक्षित करना होगा, बचाना होगा। विज्ञान के ज्ञान को प्रकृति संरक्षण में लगाना होगा। समावेषी विकास की रणनीति अपनानी होगी। ’’सस्टेने बिल डबलपमेंट’’ का सिद्धान्त अपनाना अनिवार्य है। संरक्षण से जुड़ी लघु खनिज नीति अपनानी होगी। खनन कार्य से वनों, नहरों व नदियों को होने वाली क्षति को बचाना होगा। अल्पकालीन लाभ व रोजगार के स्थान पर स्थायी आजीविका पर ध्यान देना होगा। गॉववासियों की स्थायी आजीविका का आधार खेत, चरागाह, जलस्त्रोत व वन हैं। इनका ध्यान रखना होगा। प्रकृति के संरक्षण से ही गॉव व किसान के हितों का संरक्षण होगा, यह समझना होगा। गॉव के विकास को पर्यावरण संरक्षण के व्यापक हितों से जोड़ना होगा।
पर्यावरणीय हितों से ज्यादा अनुकूल आर्गेनिक खेती और उससे जुड़ी योजनाओं के विकास की आवश्यकता है। आर्गेनिक खेती का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम रसायनों, उर्वरकों पर नियंत्रण लगाते हुए स्वस्थ कृषि इको सिस्टम विकसित करना है। लगातार कम हो रही मिट्टी क उर्वरा क्षमता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। महानगरीय वायुमंडल के लगातार जहरीले होते जाने को बचाने की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने आर्थिक नीति के महत्व पर विचार प्रकट करते हुए कहा था ’’हम तेजी से प्रगति करने के लिए बैचेन और अधीर हैं लेकिन तेजी से बढ़ने व चन्द जोखिम उठाने का मतलब यह नहीं है कि हम मूर्खतापूर्ण तरीके से बिना सोचे समझें, बिना तैयारी और बिना किसी योजना के काम करें’’ इसीलिए नेहरू ने विकास की संकल्पना में नियोजित अर्थ व्यवस्था को तरजीह दी थी। तीव्र विकास व औघोगिकरण की प्रकिया में बुनियादी बातों व सरकार के मकसद को नहीं भुलाया था। इससे विकास योजनाओं को पर्याप्त सफलता भी मिली।
यदि मनुष्य व प्राणियों को बचाना है तो संतुलित विकास से पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। जीवन षैली व विकास की अवधारणा को बदलना होगा। श्रम व उद्योग का वैकल्पिक ढ़ांचा तैयार करना होगा। प्रकृति को जीत कर भोग के लिए नष्ट करने की बजाय़, योग केन्द्रित संस्कृति व मूल्यपरक जीवनषैली अपनानी होगी। प्रकृति के साथ समरसता व सहयोग का रिष्ता कायम करना होगा।
-डा.सत्यनारायण सिंह