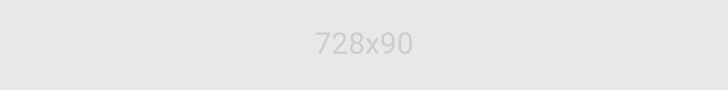हिंदी पर बढ़ता विरोध: राजनीति, अस्मिता और आंकड़ों की तहक़ीक़ात
हिंदी, जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश को जोड़ने की भाषा बनी थी, आज़ादी के 75 साल बाद एक बार फिर बहस के केंद्र में है। लेकिन इस बार बहस भाषा की उपयोगिता या सांस्कृतिक विरासत को लेकर नहीं, बल्कि हिंदी के ‘वर्चस्व’ के कथित भय और राजनीतिक लाभ के गणित पर केंद्रित है। दक्षिण भारत से शुरू हुआ यह विरोध अब महाराष्ट्र और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच चुका है। सवाल यह है कि हिंदी विरोध की यह लहर समाज से उपजी है या राजनीतिक रणनीति की प्रयोगशाला में रची गई साज़िश? भारत में संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हालांकि यह राष्ट्रभाषा नहीं है, जैसा कि आम धारणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 44% भारतीय हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। यदि इसमें हिंदी परिवार की बोलियों (अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ब्रज आदि) को शामिल करें तो यह आंकड़ा करीब 57% तक पहुंचता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, संसद और नौकरशाही के स्तर पर 60% से अधिक संप्रेषण हिंदी में होता है, जबकि शेष में अंग्रेज़ी और अन्य भारतीय भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। रेलवे, बैंकिंग, सेना और प्रशासनिक परीक्षा जैसे क्षेत्रों में हिंदी का व्यवहारिक महत्व स्पष्ट है। हिंदी विरोध कोई नया नहीं। 1965 में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश हुई, तब तमिलनाडु में जबरदस्त विरोध हुआ। उस दौर की डीएमके और द्रविड़ आंदोलन ने इसे “हिंदी साम्राज्यवाद” का नाम देकर दक्षिण भारत में मजबूत पकड़ बना ली। यह आंदोलन इतना प्रभावी रहा कि आज भी तमिलनाडु की कोई भी सरकार हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य नहीं करती। अब यही रणनीति महाराष्ट्र जैसे राज्य में दोहराई जा रही है। शिवसेना (उद्धव गुट) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (राज ठाकरे) अब हिंदी भाषियों के खिलाफ ‘मराठी अस्मिता’ की रक्षा का राग अलाप रहे हैं। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में हिंदी माध्यम की स्कूलों की संख्या बढ़ने पर सवाल उठाए गए। 30 जून 2024 को विधानसभा में विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया कि बीएमसी की नई स्कूलों में मराठी की जगह हिंदी और अंग्रेज़ी क्यों प्राथमिकता पा रही हैं? यह विरोध तब और संदिग्ध हो जाता है जब वही नेता हिंदी फिल्मों में अभिनय करते हैं, हिंदी चैनलों पर दिखते हैं और उत्तर भारतीयों के वोट से सांसद या विधायक बनते हैं। हिंदी विरोधी दलों का मुख्य तर्क है कि हिंदी को ‘थोपी’ जा रही है। लेकिन आंकड़े इस दावे की पुष्टि नहीं करते। नई शिक्षा नीति 2020 में किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। तीन-भाषा फार्मूला राज्यों की सहमति से लागू होता है, न कि जबरन। सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय जैसे राष्ट्रीय बोर्डों में भी क्षेत्रीय भाषाओं को समुचित स्थान प्राप्त है। उदाहरणस्वरूप, केरल में सीबीएसई स्कूलों में मलयालम एक अनिवार्य भाषा है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण होता है, हिंदी का हिस्सा केवल 32% है। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदी की कोई एकाधिकारवादी स्थिति नहीं है। दरअसल, हिंदी को समझने और बोलने वालों की संख्या अधिक होने के कारण उसका व्यवहारिक फैलाव ज्यादा है, न कि थोपे जाने के कारण।दरअसल, हिंदी का विरोध बहुधा उन क्षेत्रों में उठता है जहां अप्रवासी हिंदी भाषी लोग आर्थिक, व्यावसायिक या सामाजिक रूप से प्रभावशाली हो जाते हैं। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, और हैदराबाद जैसे शहरों में उत्तर भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो स्थानीय राजनीति के लिए चुनौती बनते हैं। ऐसे में भाषा का उपयोग एक सामाजिक विभाजन रेखा के रूप में किया जाता है। राजनीति इस विभाजन को भुनाती है – “बाहरी बनाम स्थानीय”, “हिंदी बनाम मातृभाषा”, और “अभिजात बनाम आम नागरिक” जैसी धारणाएं उभारी जाती हैं। इस खेल में सबसे अधिक नुकसान देश की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सौहार्द्र को होता है।भाषाओं के सहअस्तित्व को संवैधानिक और प्रशासनिक संरक्षण मिलना चाहिए। किसी भी भाषा को ‘शत्रु’ के रूप में चित्रित करना भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए आत्मघाती होगा। राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि भाषाएं संवाद का माध्यम हैं, हथियार नहीं। यदि हिंदी भाषियों को बार-बार निशाना बनाया जाएगा, तो उत्तर भारत में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया होगी, जो राष्ट्र की एकता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। शिक्षा नीति और सरकारी प्रक्रियाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेज़ी का संतुलित प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। आज का हिंदी विरोध ‘सांस्कृतिक आत्मरक्षा’ से अधिक राजनीतिक आत्म-रक्षा का यत्न है। भारत की विविधता में एकता की अवधारणा भाषा की सहअस्तित्व पर ही टिकी है। यदि इसे राजनीतिक प्रयोगशाला में बार-बार घसीटा जाएगा तो राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को भारी क्षति हो सकती है। हिंदी को थोपिए नहीं, लेकिन बांटिए भी नहीं। भाषाएं सेतु हैं, उन्हें दीवार न बनने दें।
दीपक शर्मा ‘आज़ाद’
(समसामयिक राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र टिप्पणीकार)