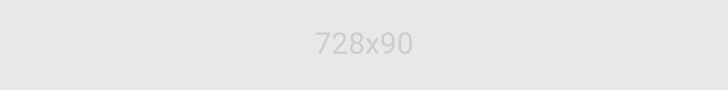हवा को जहर बनाता दिल्ली का आत्मघाती प्रदूषण
दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक बार फिर दुनिया की नजरों में भारत की राजधानी को शर्मसार कर रहा है। कभी संस्कृति, ऊर्जा और प्रगति की पहचान रही दिल्ली आज धुएं और धूल की चादर में लिपटी दिखाई देती है। हवा में घुला ज़हर इस हद तक बढ़ चुका है कि सांस लेना भी एक जोखिम बन गया है। हाल ही में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 345 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया जो “बहुत खराब” से “गंभीर” श्रेणी में आता है। यह स्थिति न केवल दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि यह भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के लिए गहन चिंतन का विषय भी है। प्रश्न यह है कि क्यों हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली का आसमान धुंधला हो जाता है और जीवन दम घोंटने लगता है। इसका उत्तर जटिल है क्योंकि इसके लिए सरकार, समाज और व्यक्ति सभी जिम्मेदार हैं। दिल्ली की गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में होना हमारे विकास के मॉडल पर एक गंभीर टिप्पणी है। जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल होने पर श्वसनतंत्र के रोगियों को किस संत्रास से गुजरना पड़ा होगा, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। यह स्थिति अन्य अनेक असाध्य रोगों का भी कारण बनती है।
प्रदूषण के प्रमुख कारणों में सबसे आगे है पराली जलाना। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा खेतों में बची फसल के अवशेष जलाने से हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा खतरनाक रूप से बढ़ जाती है। हवा की दिशा दिल्ली की ओर होती है जिससे यहाँ प्रदूषण का स्तर तेजी से चढ़ता है। इसके साथ ही दिल्ली की सड़कों पर चल रहे लाखों वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, खुले में कचरा जलाना और जनसंख्या का दबाव इस संकट को और गहरा करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली अब ‘विकास’ के नाम पर अपने ही अस्तित्व को निगलने लगी है। इस वर्ष एक बार फिर दीपावली के पटाखों ने प्रदूषण का चरम स्तर पर पहुंचा दिया है। भले ही कतिपय सामाजिक व धार्मिक संगठनों के सबल आग्रह के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सिर्फ पर्यावरण को कम हानि पहुंचाने वाले ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन प्रदूषण का स्तर बता रहा है कि यह प्रयास विफल रहा है। लोगों ने ग्रीन पटाखों की आड़ में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जमकर फोड़े हैं। जो लोगों के आत्मघाती व्यवहार का ही परिचायक है। वैसे पर्यावरणविदों का मानना है कि ग्रीन पटाखे प्रदूषण नहीं फैलाते, यह सोच तार्किक नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस तर्क से सहमत हुआ जा सकता है।
फिर भी यह कहना भी उचित नहीं कि सरकारें कुछ नहीं कर रहीं। केंद्र और राज्य सरकारों ने पिछले वर्षों में कई योजनाएँ शुरू की हैं। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने एवं भाजपा की सरकार बनने के बाद इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के उपक्रम हो रहे हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) लागू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रदूषण के स्तर के अनुसार चरणबद्ध नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दी गई, हजारों ई-बसें चलाई गईं, स्मॉग टावर लगाए गए और “ग्रीन दिल्ली ऐप” के माध्यम से शिकायतों के समाधान की व्यवस्था की गई। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए किसानों को वैकल्पिक मशीनें उपलब्ध कराई गईं और सब्सिडी दी गई। इन प्रयासों से कुछ हद तक राहत तो मिली, परंतु समस्या की जड़ अब भी जस की तस है क्योंकि यह समस्या केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक भी है।
हम कभी पराली जलाने और कभी पटाखे छोड़ने को इस संकट का कारण बताते हैं, लेकिन वास्तव में प्रदूषण के कारक हमारे तंत्र की नाकामी में हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के अधिकांश इलाकों में एक्यूआई तीन सौ पचास का आंकड़ा पार कर गया। दीपावली के बाद भी हवा का जहरीला बना रहना बेहद गंभीर विषय है। शायद वजह यह भी हो कि लोगों ने कुछ इलाकों में दो दिन दिवाली मनाई। लेकिन इस सारे प्रकरण में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कवायदें भी निष्फल ही नजर आईं। ग्रैप-2 का लागू होना स्थिति की गंभीरता को ही दर्शाता है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत होने पर वायु गुणवत्ता का संकट गहराने लगता है। जो दिल्ली की दिवाली के बाद प्राणवायु को ही दमघोंटू बनाने लगता है। हर साल शीर्ष अदालत की सक्रियता और सरकारी घोषणाओं के बावजूद स्थिति नहीं सुधरती तो यह हमारी आपराधिक लापरवाही की परिणति भी है।
प्रदूषण बढ़ाने के अनेक कारण कठोर कानून के बावजूद यत्र-तत्र पसरे हैं। लोग अब भी खुले में कचरा जलाते हैं, अपने घरों और दुकानों के बाहर धूल फैलाते हैं, पुराने वाहनों का उपयोग जारी रखते हैं। हरियाली घटती जा रही है, वृक्ष कट रहे हैं और नए पौधे लगाने की परंपरा खत्म होती जा रही है। यह लापरवाही केवल सरकार पर दोष डालने से नहीं मिटेगी, बल्कि इसके लिए नागरिक चेतना की आवश्यकता है। यह सच है कि सरकार कानून बना सकती है, नियम लागू कर सकती है, परंतु जब तक जनता अपनी आदतें नहीं बदलेगी तब तक प्रदूषण पर काबू पाना असंभव है। यदि हम अन्य महानगरों से तुलना करें तो दिल्ली की स्थिति सबसे दयनीय है। मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता की तुलना में यहाँ प्रदूषण का स्तर दोगुना से भी अधिक है। इसका कारण यह है कि दिल्ली न केवल स्थानीय प्रदूषण झेलती है बल्कि पड़ोसी राज्यों के प्रभाव में भी आती है। इसलिए समाधान भी क्षेत्रीय स्तर पर ही संभव है। केंद्र सरकार को राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर स्थायी नीति बनानी होगी ताकि पराली प्रबंधन, निर्माण नियंत्रण, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों की नीति पर एकरूपता लाई जा सके।
इस समय आवश्यकता है कि प्रदूषण को सिर्फ मौसमी समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपदा के रूप में देखा जाए। जनता में पर्यावरणीय चेतना को विद्यालयों, संस्थाओं और धार्मिक संगठनों के माध्यम से फैलाया जाए। हर कॉलोनी में ‘ग्रीन जोन’ विकसित हों, शहरी वनों का निर्माण हो, और हर व्यक्ति साल में कम से कम एक पेड़ लगाने का संकल्प ले। सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और पुराने डीजल वाहनों को सख्ती से हटाया जाए। निस्संदेह, दिल्ली के प्रदूषण में अकेले पटाखों की ही भूमिका नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ती आबादी का बोझ, हर साल बनने वाले एक लाख मकानों के निर्माण से फैलने वाला प्रदूषण तथा प्रतिवर्ष सड़कों पर उतरने वाली लाखों गाड़ियों का उत्सर्जन भी शामिल है। एक नागरिक के रूप में हमारा गैरजिम्मेदार व्यवहार इस संकट को बढ़ाने वाला है।
दिल्ली का यह प्रदूषण दरअसल हमारे विकास मॉडल की असफलता का आईना है, जहाँ हमने सुविधाओं को तो बढ़ाया पर जीवन की मूलभूत आवश्यकता-स्वच्छ हवा को खो दिया। यह केवल सरकार की विफलता नहीं बल्कि समाज की सामूहिक असंवेदनशीलता का भी परिणाम है। यदि अब भी हमने चेतना नहीं दिखाई तो आने वाली पीढ़ियाँ स्वच्छ हवा को केवल इतिहास की किताबों में पढ़ेंगी। अब समय है कि हम राजनीति, दोषारोपण और उदासीनता से ऊपर उठकर सांस लेने के अधिकार के लिए एकजुट हों। क्योंकि प्रकृति का शोषण नहीं, संरक्षण ही सभ्यता की पहचान है और यदि हमने हवा को जहर बना दिया तो हमारे सारे विकास के प्रतीक बेमानी हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब तक लोगों को यह अहसास नहीं होगा कि त्योहार के नाम पर जमकर जहरीले पटाखे छुड़ाना एक आत्मघाती कदम है, तब तक कोर्ट और सरकार के प्रयास विफल ही साबित होंगे। इसके लिए देश के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को साझी पहल करनी होगी। यह संकट सिर्फ दिल्ली या एनसीआर का नहीं है, मुंबई, कोलकाता आदि अनेक महानगरों के घातक प्रदूषण की चपेट में आने की खबरें हैं।
-ललित गर्ग