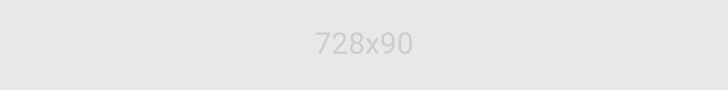माता-पिता नहीं, अभिभावक: ट्रांस अधिकारों की नई पहचान
[नालसा से केरल हाई कोर्ट तक: ट्रांस अधिकारों की विकसित होती यात्रा]
केरल हाई कोर्ट का हालिया फैसला, जिसमें ट्रांसजेंडर दंपती ज़िया और ज़हद को उनकी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में 'माता' और 'पिता' के बजाय 'अभिभावक' के रूप में दर्ज करने की अनुमति दी गई, न केवल एक कानूनी मील का पत्थर है, बल्कि सामाजिक समावेशिता और लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। यह फैसला भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने और उनके परिवार को कानूनी वैधता प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। इसने न केवल ज़िया और ज़हद के परिवार को एक नई पहचान दी, बल्कि देश भर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सामाजिक और कानूनी स्वीकृति की राह को और प्रशस्त किया।
ज़िया और ज़हद, जो केरल के कोझिकोड के रहने वाले हैं, ने 2023 में उस समय सुर्खियां बटोरीं जब ज़हद, एक ट्रांस पुरुष, ने एक बच्ची को जन्म दिया। यह भारत में पहली बार था जब एक ट्रांसजेंडर दंपती ने जैविक रूप से बच्चे को जन्म दिया। इस जोड़े ने अपनी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में अपनी पहचान को 'माता' और 'पिता' के बजाय 'अभिभावक' के रूप में दर्ज करने की मांग की, ताकि उनकी लैंगिक पहचान और सामाजिक जीवन के साथ यह दस्तावेज़ सुसंगत रहे। कोझिकोड नगर पालिका ने उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस ज़ियाद रहमान की अगुवाई वाली बेंच ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए निगम को निर्देश दिया कि वह दो महीने के भीतर संशोधित जन्म प्रमाण पत्र जारी करे, जिसमें माता-पिता के कॉलम को हटाकर याचिकाकर्ताओं को बिना लिंग उल्लेख के 'अभिभावक' के रूप में दर्ज किया जाए। यह फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है।
सबसे पहले, इस फैसले ने ट्रांसजेंडर दंपती को एक परिवार के रूप में कानूनी मान्यता दी। परंपरागत रूप से, भारतीय समाज और कानून ने परिवार की परिभाषा को पुरुष और महिला की द्वैधता (बाइनरी) के आधार पर देखा है। लेकिन यह फैसला इस रूढ़िगत धारणा को चुनौती देता है और परिवार की अवधारणा को अधिक समावेशी बनाता है। यह न केवल ज़िया और ज़हद के लिए, बल्कि समस्त ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बड़ी जीत है, जो अब अपने परिवार को कानूनी रूप से स्थापित करने का हक हासिल कर सकते हैं। यह फैसला समाज को यह संदेश देता है कि परिवार की संरचना केवल लिंग पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रेम, देखभाल और जिम्मेदारी पर आधारित होनी चाहिए।
दूसरा, यह फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय की उस मांग को और मजबूती देता है, जिसमें वे बच्चों को गोद लेने और पालने के अधिकार की वकालत करते हैं। हालांकि, भारत में गोद लेने के कानून अभी भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जटिल बने हुए हैं, लेकिन केरल हाई कोर्ट का यह फैसला एक उम्मीद की किरण है। यह न केवल जैविक माता-पिता के रूप में उनकी पहचान को मान्यता देता है, बल्कि भविष्य में गोद लिए गए बच्चों के लिए भी उनकी अभिभावक की भूमिका को स्वीकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसा कि केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील पद्मा लक्ष्मी ने कहा, यह फैसला अन्य ट्रांसजेंडर जोड़ों को बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने परिवार को बनाने और जीने के लिए प्रेरित करेगा। यह सामाजिक स्वीकृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में बराबरी का स्थान देने में मदद करेगा।
इस फैसले की जड़ें 2014 के सुप्रीम कोर्ट के नालसा (नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ) फैसले में निहित हैं। नालसा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी और उनके अधिकारों को पुरुषों और महिलाओं के समान माना था। इसने अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समानता, भेदभाव से मुक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया। केरल हाई कोर्ट का फैसला नालसा के इस आधार को और विस्तार देता है, खासकर परिवार और अभिभावक की पहचान के संदर्भ में। यह दर्शाता है कि कानून को बदलते सामाजिक मूल्यों और लैंगिक पहचान की नई समझ के साथ विकसित होना चाहिए। जस्टिस ज़ियाद रहमान ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कानून स्थिर नहीं रह सकता; उसे समाज और व्यक्तियों के जीवनशैली में आए बदलावों के अनुरूप ढलना होगा।
इसके अलावा, यह फैसला ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यावहारिक समस्याओं को भी संबोधित करता है। ज़िया और ज़हद ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि जन्म प्रमाण पत्र में उनकी लैंगिक पहचान को गलत तरीके से दर्शाने से उनकी बेटी को भविष्य में स्कूल में दाखिले, आधार कार्ड, पासपोर्ट, नौकरी और अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने इस चिंता को गंभीरता से लिया और इसे सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखा। यह एक ऐसी मिसाल है, जहां अदालत ने केवल कानूनी तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सामाजिक संदर्भ में न्याय को प्राथमिकता दी।
यह फैसला न केवल कानूनी दायरे में, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को अभी भी व्यापक सामाजिक स्वीकृति की जरूरत है। जैसा कि कोर्ट ने अपने फैसले में उल्लेख किया, भले ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता मिल चुकी हो, लेकिन समाज को इसे पूरी तरह स्वीकार करने में समय लगेगा। यह फैसला उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की वास्तविकताओं को समझने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है।
ज़िया और ज़हद की कहानी भी अपने आप में प्रेरणादायक है। दो साल पहले सोशल मीडिया पर उनकी प्रेग्नेंसी की तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींचा था। उस समय उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी इस कानूनी लड़ाई ने न केवल उनके लिए, बल्कि उन सभी ट्रांसजेंडर जोड़ों के लिए रास्ता खोला है, जो अपने परिवार को बनाने और उसे कानूनी मान्यता दिलाने का सपना देखते हैं। उनकी वकील पद्मा लक्ष्मी, जो स्वयं ट्रांसजेंडर हैं, ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी पैरवी ने न केवल इस जोड़े को न्याय दिलाया, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया।
हालांकि, यह फैसला कुछ सीमाओं के साथ आता है। कोर्ट ने इसे एक 'दुर्लभ और असाधारण' मामले के रूप में देखा और जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 में व्यापक बदलाव करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि भविष्य में ट्रांसजेंडर दंपतियों को इसी तरह की राहत पाने के लिए अलग-अलग मुकदमे लड़ने पड़ सकते हैं। फिर भी, यह फैसला एक मिसाल कायम करता है, जो भविष्य में कानून में संशोधन और अधिक समावेशी नीतियों के लिए आधार तैयार कर सकता है। केरल हाई कोर्ट का यह फैसला न केवल ज़िया और ज़हद के लिए, बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय और भारतीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह लैंगिक पहचान, परिवार और सामाजिक न्याय की नई परिभाषा गढ़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि कानून और समाज को एक-दूसरे के साथ कदमताल करना होगा, ताकि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता के साथ जीने का अधिकार मिले।
प्रो. आरके जैन “अरिजीत”, बड़वानी (मप्र)