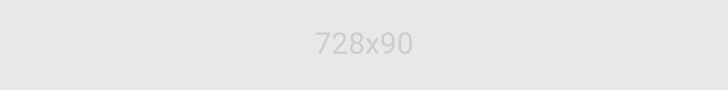विश्व वायु दिवस: चेतावनी, उम्मीद और संकल्प
हर सुबह, जब पहली सांस हमारे फेफड़ों में उतरती है, तो वह सिर्फ हवा नहीं, बल्कि जीवन की वह धड़कन है, जो हमें इस धरती की हर सजीव लय से जोड़े रखती है। यह वायु — न दिखने वाली, न छूने वाली, फिर भी हर पल हमारे होने की नींव — प्रकृति का वह अनमोल रत्न है, जो हमें बिना माँगे मिलता है। लेकिन जब यही हवा ज़हर बनकर हमारे गले को घोंटने लगती है, तो वह चीख-चीखकर पूछती है: “तुमने मेरी पवित्रता को क्यों लूटा?” विश्व वायु दिवस, जो हर साल 15 जून को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के तत्वावधान में मनाया जाता है, हमें इस सवाल से रूबरू करता है और उस धरोहर को बचाने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन हमें चेताता है कि स्वच्छ हवा कोई सौदा नहीं, बल्कि वह जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसके बिना न हमारा आज बचेगा, न हमारा कल।
आधुनिक युग की चकाचौंध ने हमें सुख-सुविधाएँ दीं, लेकिन बदले में हमारी सांसें छीन लीं। औद्योगीकरण की चिमनियों से निकलता काला धुआँ, शहरीकरण की बेलगाम दौड़, और प्राकृतिक संसाधनों का बेरहम दोहन — इन सबने हमारी हवा को एक मूक हत्यारा बना दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की 2022 की एक दिल दहलाने वाली रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 99% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है, जो डब्ल्यूएचओ के वायु गुणवत्ता मानकों से कहीं अधिक दूषित है। इस प्रदूषण के कारण हर साल करीब 70 लाख लोग असमय मृत्यु का शिकार हो रहे हैं — 40 लाख बाहरी वायु प्रदूषण से, और 30 लाख घरेलू प्रदूषण से। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5 और पीएम10) जैसे ज़हरीले तत्व हमारे फेफड़ों को जकड़ रहे हैं। ये तत्व अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग, और फेफड़ों के कैंसर जैसी घातक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। खासकर पीएम2.5, जो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण हैं, रक्तप्रवाह में घुसकर बच्चों की कोमल सांसों और बुजुर्गों की कमज़ोर धड़कनों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं।
यह संकट किसी एक कोने तक सीमित नहीं। दिल्ली, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है, इसका एक दर्दनाक उदाहरण है। आईक्यूएयर की 2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली का एक्यूआई अक्सर 300 को पार कर ‘खतरनाक’ स्तर पर पहुँच जाता है, जहाँ सांस लेना भी एक जंग बन जाता है। लेकिन यह ज़हर अब केवल शहरों तक नहीं रुका। भारत के गाँवों में पराली जलाने, बायोमास चूल्हों, और पारंपरिक ईंधन से निकलने वाला धुआँ हवा को दमघोंटू बना रहा है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, भारत में घरेलू वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 10 लाख लोग अपनी जान गँवाते हैं। बीजिंग, लाहौर, और मेक्सिको सिटी जैसे शहर भी इस अदृश्य आपदा से त्रस्त हैं। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और भयावह बना दिया है। बढ़ता तापमान और मौसमी उथल-पुथल प्रदूषकों को और ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं, जिससे हवा में ज़हर का जाल और घना हो जाता है।
इस आपदा से निपटने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ सरकारों या पर्यावरणविदों की नहीं, बल्कि हम सबकी है। हमारी छोटी-छोटी कोशिशें बड़े बदलाव की नींव रख सकती हैं। निजी वाहनों का कम उपयोग, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन को अपनाना, ऊर्जा की बचत, और वृक्षारोपण जैसे कदम हवा को शुद्ध करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से भी लड़ते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, अगर भारत में 10% लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन चुनें, तो कार्बन उत्सर्जन में 15-20% की कमी आ सकती है। एक परिपक्व पेड़ सालाना 20 किलोग्राम CO2 सोखता है, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। नीतिगत स्तर पर, सरकारों को कठोर कदम उठाने होंगे। भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) 122 शहरों में पीएम2.5 और पीएम10 के स्तर को 20-30% कम करने का लक्ष्य रखता है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। उद्योगों पर सख्त प्रदूषण नियंत्रण, सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों में निवेश, और पर्यावरण-केंद्रित शहरी नियोजन अब टाले नहीं जा सकते। डेनमार्क और जर्मनी जैसे देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा अपनाकर दिखाया है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना असंभव नहीं।
शिक्षा और जागरूकता इस जंग का सबसे ताकतवर हथियार हैं। स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ हवा की कीमत सिखाना, युवाओं को हरित तकनीकों में नवाचार के लिए प्रेरित करना, और समाज को यह समझाना कि पर्यावरण की रक्षा आत्मरक्षा है — यह एक क्रांति की शुरुआत कर सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2020 का लॉकडाउन इसका जीवंत सबूत है, जब कुछ ही हफ्तों में दिल्ली का एक्यूआई 300 से घटकर 50-100 तक आ गया, और हिमालय की चोटियाँ पंजाब से चमकने लगीं। यह बताता है कि अगर हम चाहें, तो स्वच्छ हवा का सपना हकीकत बन सकता है।
वायु प्रदूषण सिर्फ़ पर्यावरण का मसला नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक संकट भी है। यह सबसे ज़्यादा गरीब और कमज़ोर वर्गों को प्रभावित करता है, जो स्वच्छ हवा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। यूएनईपी की 2025 की थीम “क्लीन एयर फॉर ऑल” हमें याद दिलाती है कि स्वच्छ हवा हर इंसान का हक है, और इसकी ज़िम्मेदारी हम सबकी है। हमारी हर सांस एक-दूसरे से जुड़ी है, और हमारा हर कदम पूरी मानवता को प्रभावित करता है।
अगली बार जब आप सांस लें, तो उस हवा को महसूस करें जो आपको जीवित रखती है। यह न सोचें कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। हर पेड़ जो आप लगाते हैं, हर साइकिल जो आप चलाते हैं, हर आवाज़ जो आप पर्यावरण के लिए उठाते हैं, वह एक नई सुबह की शुरुआत है। विश्व वायु दिवस हमें वह चिंगारी जलाने का मौका देता है, जो हमारी धरती को फिर से हरा-भरा और हमारी सांसों को फिर से आज़ाद कर सकती है। आज यह संकल्प लें कि हम न केवल अपने लिए, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी दुनिया बनाएँगे, जहाँ हर सांस एक उत्सव हो, हर श्वास एक गीत। क्योंकि अगर सांसें रुक गईं, तो सब रुक जाएगा। लेकिन अगर हमने आज हवा को बचा लिया, तो हमने जीवन को, भविष्य को, और इस धरती की हर धड़कन को बचा लिया।